

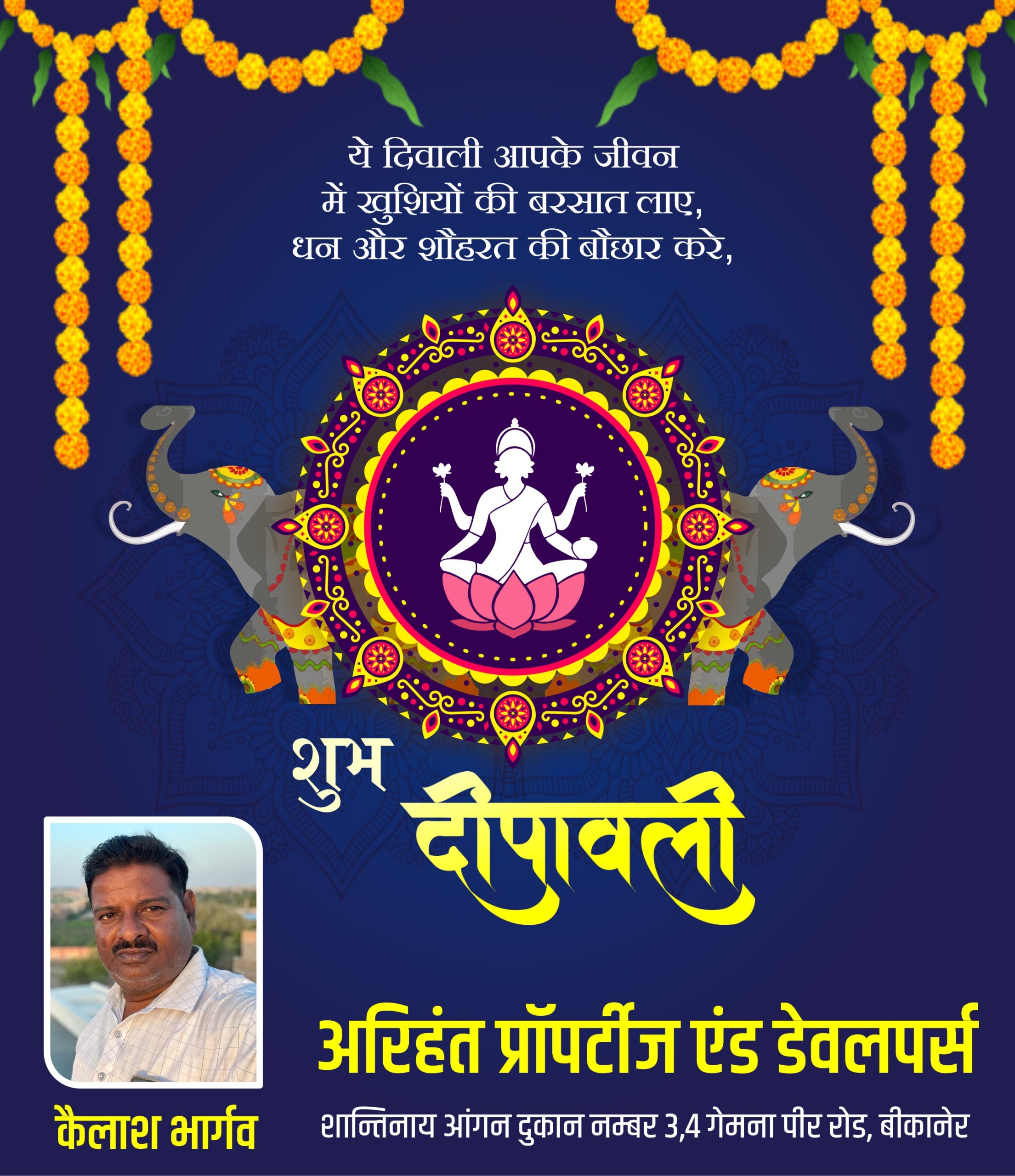



मनमीत
कल कोविद ने तीस रुपये माँगे। मैंने कहा क्या लाएगा। बोला पाँच बूमर एक मीनाक्षी ( मुरमुरे ) दो दस-दस वाले कुरकुरे। मैंने कहा पेंट की जेब में खुल्ले रुपये हैं ले जा। और अकेला मत खाना। मैं भी खाऊंगा और यामी भी। बोला ठीक है। पंद्रह मिनट बाद हाँफता हुआ आया। मैंने कहा क्या हुआ। बोला दस रुपये गिर गए। सॉरी। मैंने कहा कोई नहीं लेकिन गिरे कैसे? बोला बकरियों का रेवड़ जा रहा था। मैं बकरियों से खेलने लगा। पता नहीं कैसे छूट गया एक नोट। और यह कहकर उदास हो गया। मैंने कहा जो गिर गया सो गिर गया। अब सामान तो दे। उसने एक कुरकुरे का पैकेट मुझे दे दिया। मैं चाय बनाने चला गया।
दस मिनट बाद वो फिर आया। इस बार चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ। मैंने कहा अब क्या हुआ?
बोला आप दुखी तो नहीं हो ना? आप उदास तो नहीं ना कि आपके रुपये गिर गए?
मैं हैरान कि ग्यारह बरस की उम्र में इतनी सेंसेटिविटी कहाँ से आ गई इसमें? इतना अपराधबोध?
और वो रोने लगा। इधर मैं भी। रोना धोना कोई दो मिनट चला होगा। मेरे भीतर एक अलार्म बजने लगा!
मुझे लगा कि इस बच्चे को माँ सरस्वती ने चुन लिया है!
किसी कला के लिए। अपने मूल में वरदान मगर बाहर से एक शाप या मूल में शाप और बाहर से वरदान। पता नहीं! मगर चुन तो लिया है।
(2)
कुछ लोगों के लिए लोग शिकार-भर होते हैं और जहाँ तक वे देख सकते हैं वह एक शिकारगाह!
वे हर दिन एक नया शिकार करते हैं। उसे ज्ञान, अहम, तत्सम, स्मृति, परम्परा, संवेदना, लोलुपता और करुणा रूपी भाले के फाल से घायल करते हैं और उसे अपनी इच्छा की आग में जीवित भूनते हैं। फिर कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह सचमुच उनके भाले की नोक पर है या नहीं। उनको प्रधानमंत्री को भूनना होता है मगर वे किसी राकेश सुरेश मनमीत जगजीत अशोक किशोर आदि को प्रधानमंत्री की जगह चुनकर भून लेते हैं।
और यह बेचारे लोग कुछ समय के लिए विचलित भी हो जाते हैं।
हाँलाकि उनके दिन भर के शिकार का परिणाम रात को उन्हीं के भीतर एक अवसाद भरी मृत्यु निकलता है। लेकिन वे अगली सुबह फिर जाग जाते हैं। उतने ही आक्रामक, उतने ही चौकन्ने और उतने ही कृतघ्न।
यह संसार ऐसे लोगों के होते शिकारगाह से अभयारण्य में कभी नहीं बदल सकता।
(3)
दीवाली के दिनों में घर की सफाई के नाम पर अपनी माँ को बुरी तरह थकते हुए देखता हूँ। जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आधे काम ग़ैर ज़रूरी हैं; लेकिन माँ अपने भीतर का सारा अस्त-व्यस्त घर के अस्त-व्यस्त में उँड़ेल देती है – और घर के अस्त-व्यस्त को ठीक करके उसे लगता है उसने अपने भीतर के अस्त-व्यस्त को ठीक कर लिया है। जब तक वह ससुराल में अपनी सास के अंडर थी उसकी मज़बूरी समझ आती थी मगर अब तो ख़ुद का घर है। यह कंडीशनिंग कितनी गहरी है। मैं उसकी महान ऊर्जा का अपव्यय होते देखता रहता हूँ। हाथ बंटाऊ तो वह इससे भी राज़ी नहीं कि मेरा बेटा यह सब काम करे। वह हर दिन ख़र्च हो रही है और उसकी उम्र कम हो रही है। यह बात सोचकर मैं कांप जाता हूँ।
क्या अंतर पड़ता है कि कुछ ख़ाली डिब्बे इस बरस भी अनफेंके रह गए। क्या अंतर पड़ता है कि टाण पर पुराने कपड़ों की एक गठरी गरीबों में बांटे बिना रह गई। क्या अंतर पड़ता है कि टाइल पर अब भी कुछ दाग़ बाक़ी हैं।
छीजती जाती है खीजती जाती है हाँफ़ती जाती है।
दुर्भाग्य! अन्याय! मूर्खता!
दीवाली पर अगर घर की स्त्रियां ही काम करते-करते बुझने लगें तो फिर इस त्यौहार की जगमग का क्या अर्थ रह जाता है?

